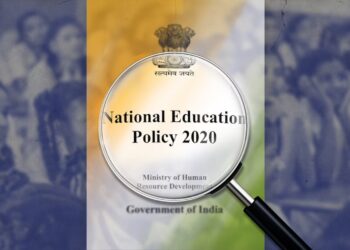अमित पांडे: संपादक
दिल्ली के एक शिक्षा सम्मेलन में भारत सरकार के स्कूल शिक्षा सचिव संजय कुमार, आईएएस, ने जो वक्तव्य दिया, वह सतही तौर पर एक सामान्य आंकड़ा प्रस्तुति लग सकता है, लेकिन उसकी गूंज कहीं गहरी और चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि सरकारी सीबीएसई स्कूलों में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है, जबकि निजी सीबीएसई स्कूलों में लड़के भारी संख्या में हैं। यह कथन जितना सीधा था, उतना ही यह एक खतरनाक सच्चाई की ओर इशारा करता है—कि भारत की शिक्षा व्यवस्था धीरे-धीरे निजी हाथों में सौंप दी जा रही है। और जब यह बात एक वरिष्ठ नौकरशाह, न कि कोई राजनेता, बिना किसी प्रतिरोध के कहता है, तो यह केवल नीति की चूक नहीं, बल्कि विचारधारा की हार है।
क्या संजय कुमार को यह अधिकार है कि वे सार्वजनिक मंच से निजी शिक्षा में सरकारी निवेश की वकालत करें? यदि नहीं, तो उन्होंने उस मंच का उपयोग नए सरकारी स्कूलों की घोषणा के लिए क्यों नहीं किया, विशेषकर बालिकाओं के लिए? उन्होंने निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने या सार्वजनिक शिक्षा ढांचे को विस्तार देने की कोई योजना क्यों नहीं रखी? जब देश में पिछले कुछ वर्षों में एक लाख से अधिक सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, तब सार्वजनिक शिक्षा के विस्तार पर चुप्पी केवल चूक नहीं, बल्कि ज़िम्मेदारी से भागना है।
दिल्ली सरकार के तहत अरविंद केजरीवाल ने यह दिखाया है कि सार्वजनिक शिक्षा को सुधारा जा सकता है, उसे गरिमा दी जा सकती है, और उसे आकांक्षात्मक बनाया जा सकता है। फिर केंद्र सरकार ऐसे मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं अपना रही? यदि “सबका साथ, सबका विकास” को कोई अर्थ देना है, तो उसकी शुरुआत सार्वजनिक शिक्षा में सार्वजनिक निवेश से होनी चाहिए, न कि निजी वर्चस्व की मौन स्वीकृति से।
शिक्षा एक मौलिक अधिकार है—कोई बाज़ारू वस्तु नहीं। यदि राज्य स्वयं को एक कॉर्पोरेट एजेंट की तरह प्रस्तुत करने लगे, और अफ़सर चुनावी भाषणों की शैली में बोलने लगें, तो कल्याणकारी राज्य की आत्मा ही संकट में पड़ जाती है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए: क्या संजय कुमार का वक्तव्य उनका निजी मत था, या सरकार की नीति का संकेत? क्योंकि यदि भारत की शिक्षा का भविष्य निजी खिलाड़ियों के हवाले किया जा रहा है, तो जनता को यह बात स्पष्ट, ईमानदारी से और बिना तालियों के बताई जानी चाहिए।
और इस पूरे घटनाक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका पर भी सवाल उठता है। क्या वे इस सबको देख रहे हैं, या बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने में व्यस्त हैं? यदि उनके मंत्रालय के अधिकारी अब खुलेआम निजी शिक्षा की वकालत कर रहे हैं और जनता से उसमें निवेश की अपेक्षा कर रहे हैं, तो उन्हें यह बात बिहार की हर चुनावी सभा में गर्व से कहनी चाहिए। और यदि यह सरकार की नीति नहीं है, तो उन्हें जवाब देना चाहिए कि यह सब कैसे हुआ। क्या वे किसी सार्वजनिक मंच से यह स्पष्ट करेंगे कि क्या अब भारत में शिक्षा का संचालन निजी क्षेत्र के भरोसे होगा, क्योंकि सरकार इसे वहन करने में असमर्थ है?
यदि ऐसा है, तो फिर “सबका साथ, सबका विकास” जैसे नारों को भी बदल देना चाहिए। क्योंकि जब अफ़सर भाषण देने लगें और सरकार पीछे हट जाए, तो यह केवल नीति की विफलता नहीं, बल्कि जनकल्याण के विचार की पराजय होती है। जनता को यह जानने का अधिकार है कि क्या अब शिक्षा भी उसी निजीकरण की राह पर है, जिस पर स्वास्थ्य, परिवहन और रोज़गार पहले ही चल पड़े हैं। और यदि हाँ, तो यह बदलाव एक पारदर्शी बहस के ज़रिए होना चाहिए—ना कि अफ़सरों की तालियों से सजी मंचीय घोषणाओं के ज़रिए।