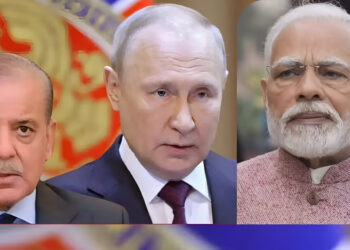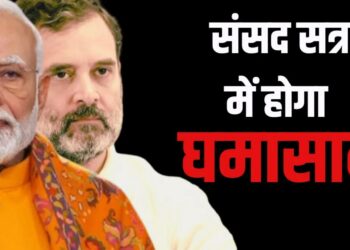अमित पांडे: संपादक
महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, वह केवल एक ज़मीन के सौदे तक सीमित नहीं है—यह उस गहरे राजनीतिक और नैतिक संकट की ओर इशारा करता है जिसमें सत्ता, जाति और लोकतंत्र की मर्यादा एक-दूसरे से टकरा रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवाल—चाहे वह मतदाता सूची में कथित हेरफेर हो या पुणे के मुंढवा क्षेत्र की 1800 करोड़ रुपये मूल्य की महार वतन ज़मीन का 300 करोड़ में कथित रूप से बेचा जाना—सिर्फ आरोप नहीं हैं, बल्कि वे उस व्यवस्था पर सवाल हैं जो दलितों के अधिकारों को सत्ता की सौदेबाज़ी में गिरवी रख देती है।
महार वतन ज़मीनें ऐतिहासिक रूप से दलित समुदाय, विशेषकर महार जाति, को दी गई थीं। इन ज़मीनों की बिक्री पर कानूनी रोक है, क्योंकि ये केवल सरकार की अनुमति से ही हस्तांतरित की जा सकती हैं। ऐसे में यदि यह आरोप सही है कि यह ज़मीन उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे रोहित पवार से जुड़ी कंपनी को बाज़ार मूल्य से कहीं कम पर बेची गई, और उस पर स्टांप ड्यूटी भी माफ़ कर दी गई, तो यह केवल आर्थिक घोटाला नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की नींव पर हमला है।
राहुल गांधी का यह कहना कि “यह ज़मीन की चोरी है, उस सरकार द्वारा की गई जो वोट की चोरी से बनी है”, एक राजनीतिक बयान भर नहीं है। यह उस व्यापक अविश्वास को दर्शाता है जो आज भारत के लोकतंत्र में पनप रहा है—जहां चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं, और जहां सत्ता में बने रहने के लिए दलितों, आदिवासियों और वंचितों के अधिकारों की बलि दी जाती है।
चुनाव आयोग द्वारा राहुल गांधी के आरोपों को “दुर्भावनापूर्ण प्रचार” कहकर खारिज कर देना, लेकिन उनके द्वारा उठाए गए तथ्यों पर कोई स्पष्ट उत्तर न देना, लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। यदि मतदाता सूची में हेरफेर हुआ है, तो उसका स्वतंत्र और पारदर्शी जांच होना लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है। और यदि नहीं हुआ, तो तथ्यों के साथ उसका खंडन होना चाहिए। चुप्पी, विशेषकर संवैधानिक संस्थाओं की, संदेह को और गहरा करती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि स्वयं आरोप। जब एक राज्य में दलितों की ज़मीन के साथ कथित धोखाधड़ी होती है, और जब उसी राज्य में चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगते हैं, तब केंद्र सरकार की नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि वह न केवल स्थिति स्पष्ट करे, बल्कि यह सुनिश्चित करे कि न्याय हो। लेकिन यदि सत्ता का गणित इस चुप्पी को आवश्यक बनाता है—क्योंकि वही नेता सत्ता में साझेदार हैं—तो यह चुप्पी केवल राजनीतिक नहीं, नैतिक पतन का संकेत बन जाती है।
इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू है—दलित अधिकारों का संस्थागत क्षरण। जब आरक्षित ज़मीनें बाज़ार की वस्तु बन जाएं, जब वंचित समुदायों के लिए सुरक्षित संसाधन सत्ता के गलियारों में सौदेबाज़ी का हिस्सा बनें, तो यह केवल एक समुदाय का नहीं, पूरे संविधान का अपमान है। यह वही संविधान है जिसने दलितों को अधिकार दिए, उन्हें ज़मीन, शिक्षा और प्रतिनिधित्व में हिस्सेदारी दी। यदि आज वही अधिकार सत्ता की गठजोड़ में कुचले जा रहे हैं, तो यह केवल एक घोटाले की बात नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की हत्या है।
इसलिए यह ज़रूरी है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष, न्यायिक जांच हो। केवल प्रशासनिक समिति बनाकर या राजनीतिक बयान देकर इस मुद्दे को दबाया नहीं जा सकता। यह मामला केवल एक ज़मीन का नहीं, बल्कि उस भरोसे का है जो भारत के करोड़ों दलितों ने संविधान और लोकतंत्र पर किया है।
और अंत में, यह भी समझना होगा कि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं है। वह जवाबदेही, पारदर्शिता और न्याय की निरंतर प्रक्रिया है। यदि सत्ता में बैठे लोग यह मान लें कि वे वोट की ताक़त से किसी भी अन्याय को वैध बना सकते हैं, तो यह लोकतंत्र नहीं, बहुमत का अधिनायकवाद बन जाएगा।
इसलिए आज ज़रूरत है कि हम न केवल इस प्रकरण की सच्चाई जानें, बल्कि यह भी सुनिश्चित करें कि भारत का लोकतंत्र, उसकी संस्थाएं और उसका संविधान, किसी भी सत्ता की सुविधा का उपकरण न बनें—बल्कि वंचितों की आवाज़ और अधिकारों के संरक्षक बने रहें।