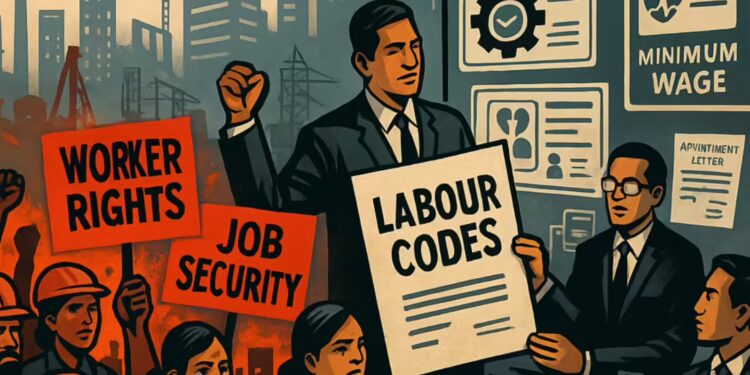अमित पांडे: संपादक
देश एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ा दिख रहा है, जहां आर्थिक सुधार के नाम पर लिए जा रहे निर्णय और श्रमिकों के अधिकारों के बीच टकराव केवल नीतिगत बहस नहीं, बल्कि राजनीतिक ध्रुवीकरण का भी कारण बन रहे हैं। चार नई श्रम संहिताओं को लागू करने की केंद्र सरकार की जल्दबाजी ने तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे विपक्ष शासित राज्यों के साथ टकराव की नई जमीन तैयार कर दी है। सवाल यह है कि क्या ये संहिताएं सचमुच श्रमिकों के हितों को मजबूत करने के लिए हैं या फिर इन्हें “ईज ऑफ डुइंग बिजनेस” के नाम पर श्रमिक सुरक्षा की परतें कमजोर करने के औजार के रूप में देखा जाना चाहिए।
केंद्र सरकार का तर्क साफ है: 29 बिखरे हुए श्रम कानूनों को समेकित कर चार व्यापक कोड के रूप में ढालना, कानूनी उलझनों को कम करना और उद्योगों के लिए स्पष्ट और सरल ढांचा तैयार करना समय की मांग है। वैश्विक निवेश आकर्षित करने और उत्पादन आधारित विकास रणनीति को गति देने के लिए श्रम कानूनों में लचीलापन लाना, सरकार की आर्थिक सोच का प्रमुख घटक बन चुका है। लेकिन यह भी कम सच्चाई नहीं कि जिस वर्ग के अधिकारों पर सबसे अधिक असर पड़ने वाला है, वही वर्ग – यानी संगठित और असंगठित मजदूर – इस पूरी प्रक्रिया में अपने को हाशिये पर महसूस कर रहा है। जब ट्रेड यूनियनों का एक व्यापक मोर्चा इन संहिताओं को “मजदूर विरोधी” कह रहा हो और विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहा हो, तो यह केवल राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि गहरे असंतोष का संकेत है।
पश्चिम बंगाल का रवैया इस पूरे विवाद की पहली परत खोलता है। पिछले पांच वर्षों से राज्य सरकार केंद्र के आग्रह के बावजूद मसौदा नियम प्रकाशित करने से परहेज कर रही है। केंद्र के सूत्र इसे राजनीतिक जिद बताकर खारिज कर सकते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लिए यह मुद्दा केवल तकनीकी नहीं, वैचारिक भी है। पार्टी का यह स्थापित रुख रहा है कि श्रम कानूनों में बदलाव इस तरह नहीं किए जा सकते कि मजदूरों की संगठित शक्ति और सौदेबाजी की क्षमता कमजोर पड़ जाए। यदि नए कोड के तहत ट्रेड यूनियन बनाने, हड़ताल करने और सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया में अतिरिक्त बाधाएं खड़ी होती हैं, तो यह स्वाभाविक है कि विपक्ष शासित राज्य इसे अपने सामाजिक न्याय के एजेंडे के खिलाफ मानें।
तमिलनाडु का रुख कुछ अलग किंतु समान रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य ने तीन संहिताओं के मसौदा नियम तो जारी कर दिए, लेकिन ‘सोशल सिक्योरिटी कोड’ पर गंभीर आपत्ति दर्ज की है। यह आपत्ति केवल राजनीतिक नहीं, व्यावहारिक भी है। दशकों से चल रही राज्य–स्तरीय कल्याण योजनाएं, जैसे असंगठित मजदूरों के लिए विशेष पेंशन, मातृत्व लाभ या स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम, केंद्र की नई संरचना में हाशिये पर चले जाएं या वित्तीय रूप से अस्थिर हो जाएं, तो राज्य सरकारों की सामाजिक जिम्मेदारी निभाना कठिन हो जाएगा। यदि श्रमिक कल्याण की जिम्मेदारी धीरे-धीरे केंद्र-नियंत्रित कानूनों और कोषों की ओर सरकती है, तो राज्यों के पास नीति नवाचार की गुंजाइश घटेगी और उनका राजनीतिक उत्तरदायित्व बढ़ते असंतोष के रूप में सामने आएगा।
केरल का उदाहरण इस बहस को और गहरा कर देता है। वाम मोर्चा सरकार ने प्रारंभ में चारों संहिताओं के मसौदे जारी कर केंद्र के साथ औपचारिक सहयोग का संकेत दिया था, लेकिन अब श्रम मंत्री का यह बयान कि “कोई भी निर्णय मजदूर अधिकारों को कमजोर कर के नहीं लिया जाएगा”, यह दिखाता है कि व्यावहारिक स्तर पर राज्य भी संभावित प्रतिकूल प्रभावों को लेकर चिंतित है। केरल जैसे राज्य, जहां ट्रेड यूनियन संस्कृति मजबूत और संगठित है, वहां किसी भी ऐसे कानून का सहज स्वीकार्य होना मुश्किल है जो औद्योगिक शांति के नाम पर मजदूरों की आवाज को नियंत्रित करने की दिशा में जाता हुआ प्रतीत हो।
इन तीनों राज्यों की राजनीतिक पृष्ठभूमि भले अलग-अलग हो, लेकिन श्रम संहिताओं पर उनका विरोध एक साझा चिंता से उपजता है कि केंद्र आर्थिक सुधारों के नाम पर संवैधानिक संघवाद की भावना को कमजोर न कर दे। श्रम विषय समवर्ती सूची में है, यानी सिद्धांत रूप में केंद्र और राज्यों को मिलकर सहमति से रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन अगर एक पक्ष केवल “परामर्श” की औपचारिकता निभाकर आगे बढ़ना चाहता हो और दूसरा पक्ष यह महसूस करे कि उसकी आपत्तियों को नीतिगत स्तर पर गंभीरता से नहीं सुना जा रहा, तो परिणाम टकराव ही होगा। यह टकराव अदालतों से लेकर सड़क तक, हर मंच पर दिख सकता है।
ट्रेड यूनियनों की भूमिका इस पूरे परिदृश्य में निर्णायक रहेगी। भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर लगभग सभी केंद्रीय संगठन इन संहिताओं के खिलाफ लामबंद हैं। उनकी चिंता यह है कि नए प्रावधान कंपनियों को रोजगार देने में तो अधिक लचीलापन देंगे, लेकिन इसका अर्थ अक्सर यही निकलेगा कि स्थायी नौकरियों की जगह अनुबंध आधारित, कम सुरक्षा वाली नौकरियां बढ़ेंगी; काम के घंटे और शर्तें बदलने के लिए नियोक्ताओं को अधिक छूट मिलेगी; और बड़े पैमाने पर छंटनी या लॉकआउट जैसी कार्रवाइयों पर पहले से कम नियामक बाधाएं रह जाएंगी। ऐसे में मजदूरों के लिए न्याय पाने का रास्ता कानूनी रूप से अधिक जटिल, महंगा और समयसाध्य बन सकता है।
केंद्र का तर्क है कि उदारीकृत श्रम बाजार अधिक निवेश और अधिक रोजगार का रास्ता खोलेगा। लेकिन यह प्रश्न लगातार पूछा जाना चाहिए कि क्या रोजगार की मात्रा बढ़ाने के लिए उसके गुणवत्ता मानकों को कम करना स्वीकार्य है। अगर विकास का मॉडल ऐसे श्रमिकों पर टिकेगा जिन्हें न्यूनतम सुरक्षा भी सुनिश्चित न हो, तो वह विकास लंबे समय तक सामाजिक स्थिरता कैसे बनाए रख पाएगा? आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को आमने-सामने खड़ा कर देने वाली नीतियां अंततः लोकतांत्रिक सहमति को कमजोर करती हैं।
यह भी ध्यान देने योग्य है कि केंद्र ने मसौदा नियमों को पुनः जारी कर सुझाव मांगने का निर्णय तब तेज किया है जब बिहार के चुनाव परिणामों ने सत्तारूढ़ गठबंधन को राजनीतिक रूप से मजबूत किया है। यह धारणा कमज़ोर नहीं है कि राजनीतिक मजबूती मिलने के बाद सरकार उन सुधारों को आगे बढ़ाने का जोखिम ज्यादा उठाती है जिन्हें वह सामान्य परिस्थितियों में टालती रहती। लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संख्या-बल और जनमत, दोनों को अलग-अलग कसौटियों पर परखा जाना चाहिए। संसद में बहुमत होने का अर्थ यह नहीं कि समाज के कमजोर वर्गों की आशंकाओं को नज़रअंदाज कर दिया जाए।
आज जरूरत इस बात की है कि श्रम संहिताओं पर बहस चुनावी नारों और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठकर हो। केंद्र अगर सचमुच इन कानूनों को ऐतिहासिक सुधार साबित करना चाहता है, तो उसे विपक्ष शासित राज्यों और ट्रेड यूनियनों के साथ ईमानदार संवाद की पहल करनी होगी। इसी तरह, राज्यों को भी केवल राजनीतिक विरोध के लिए विरोध करने के बजाय ठोस वैकल्पिक सुझाव रखने होंगे, ताकि मजदूर अधिकार और आर्थिक गतिशीलता दोनों के बीच संतुलित रास्ता खोजा जा सके।
आखिरकार परीक्षा केवल इन चार संहिताओं की नहीं है; परीक्षा इस बात की है कि भारत किस तरह का विकास मॉडल चुनता है—वह जो श्रम को केवल लागत मानकर देखता है, या वह जो श्रम को गरिमा, अधिकार और सामाजिक न्याय से जोड़कर देखता है। यही चयन आने वाले वर्षों में हमारी राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज के चरित्र को तय करेगा।