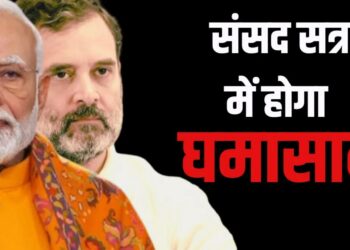अमित पांडे: संपादक
जब 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू हुआ था, तब इसे भारत की “दूसरी आज़ादी” कहा गया था — अप्रत्यक्ष करों की जटिलता से मुक्ति, एक राष्ट्र–एक कर की अवधारणा और पारदर्शी शासन की ओर एक ऐतिहासिक कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे कर क्रांति बताया था, जिसने देश को आर्थिक एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ाया। पर आज, आठ वर्ष बाद, यही व्यवस्था सवालों के घेरे में है। क्या जीएसटी सचमुच आर्थिक आज़ादी लेकर आया, या यह केंद्रीकरण और भ्रष्टाचार का नया औज़ार बन गया?
लखनऊ से हाल ही में सामने आए ₹200 करोड़ के जीएसटी घोटाले ने इस पूरे तंत्र की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने वर्षों तक राजस्व संग्रह में हेराफेरी कर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए की चोरी की। यह पूरा खेल न केवल सरकारी निगरानी तंत्र की विफलता दर्शाता है बल्कि यह भी बताता है कि डिजिटल युग में भी पारदर्शिता केवल नारे बनकर रह गई है। जब राजधानी में बैठकर अधिकारी इतने बड़े पैमाने पर गबन कर सकते हैं, तो देश के अन्य हिस्सों की स्थिति की कल्पना सहज की जा सकती है।
प्रधानमंत्री द्वारा बार-बार दोहराया गया नारा — “ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा” — अब इस घोटाले के बाद खोखला प्रतीत होता है। यह केवल अधिकारियों की लापरवाही नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की सड़ांध का प्रमाण है। अगर “रियल-टाइम मॉनिटरिंग” वाला डिजिटल सिस्टम ₹200 करोड़ के गबन का पता नहीं लगा पाया, तो सवाल उठता है कि यह तकनीकी ढांचा आखिर किसके लिए बनाया गया था — जनता की निगरानी के लिए या भ्रष्टाचार की सुरक्षा के लिए?
जांच में सामने आया है कि सहायक आयुक्तों से लेकर अतिरिक्त आयुक्तों तक, कई वरिष्ठ अधिकारी इस खेल में शामिल थे। गाज़ियाबाद, आगरा, कानपुर, मेरठ और वाराणसी जैसे ज़िलों में पोस्टिंग पाए अधिकारियों ने जीएसटी की वसूली को निजी निवेश में बदल दिया। आरोप है कि उन्होंने इन रकमों को अचल संपत्तियों में लगाया, जिसमें एक बिल्डर भी शामिल था जो एक वरिष्ठ अधिकारी का रिश्तेदार बताया जा रहा है। कोविड काल के दौरान, जब निगरानी सबसे कमज़ोर थी, तब यह “कुबेर काल” कहा जाने वाला दौर सबसे अधिक लाभदायक साबित हुआ।
उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित कर मामले की जांच शुरू की है, लेकिन जनता का विश्वास पहले ही टूट चुका है। विपक्षी दलों ने इसे शासन की नाकामी बताया है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, “इस सरकार ने भ्रष्टाचार को सुधार का नाम दे दिया है। जीएसटी को पारदर्शिता के प्रतीक के रूप में बेचा गया था, पर यह अब डिजिटल दलालों का जाल बन चुका है।”
यह घोटाला नया नहीं है, बल्कि एक लगातार चल रही श्रृंखला का हिस्सा है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं — 2019 का पुणे ई-वे बिल घोटाला (₹300 करोड़), 2021 में कर्नाटक का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाला (₹1,200 करोड़), 2022 में तमिलनाडु का ₹250 करोड़ का आईटीसी घोटाला, और 2023 में दिल्ली के वाणिज्य कर विभाग का ₹110 करोड़ रिश्वत प्रकरण। हर बार सरकार ने “कुछ बुरे अधिकारियों” को दोषी ठहराकर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया, पर व्यवस्था वैसी ही रही।
अर्थशास्त्री जयति घोष कहती हैं, “जीएसटी एक राजनीतिक परियोजना थी जिसे राजकोषीय सुधार का रूप दिया गया। इससे राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता कमजोर हुई और केंद्र के हाथ में शक्ति केंद्रित हो गई। पारदर्शिता के नाम पर अपारदर्शिता बढ़ी, और जब जवाबदेही ऊपर जाती है, तो नीचे तक दण्डमुक्ति फैलती है।”
राज्यों के मुख्यमंत्रियों — ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन और भूपेश बघेल — ने भी बार-बार जीएसटी मुआवज़े को लेकर केंद्र पर पक्षपात और नियंत्रण के आरोप लगाए हैं। उनके आरोपों को पहले राजनीति कहा गया, पर लखनऊ की घटना ने इन दावों को नया औचित्य दे दिया है।
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल “जिम्मेदारी” का है। क्या केवल अधिकारियों को दोषी ठहराना पर्याप्त है? वह प्रणाली, जिसने उन्हें वर्षों तक ऐसे पदों पर बनाए रखा, क्या दोषमुक्त है? वह राजनीतिक नेतृत्व, जिसने सतर्कता और पारदर्शिता का दावा किया, क्या अब जवाब नहीं देगा?
यह घोटाला यह भी साबित करता है कि डिजिटल गवर्नेंस का मतलब जरूरी नहीं कि ईमानदारी हो। आंकड़े बताते हैं कि 2019 से 2024 के बीच छोटे व्यापारियों के जीएसटी पंजीकरण में 38% की गिरावट आई, जबकि कर चोरी के मामलों में 44% की वृद्धि हुई। यह संकेत है कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसने डिजिटल रूप धारण कर लिया है।
सरकार अब जांच की घोषणा कर चुकी है, पर जनता को केवल जांच नहीं, परिणाम चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जीएसटी की साख बचानी है तो कुछ कठोर कदम आवश्यक हैं — जैसे कि उच्च-राजस्व वाले जिलों में अधिकारियों का दो वर्ष से अधिक कार्यकाल न हो, एक स्वतंत्र ऑडिट एजेंसी बनाई जाए जो जीएसटी संग्रह और रिफंड की निगरानी करे, राज्यों को केंद्रीय डैशबोर्ड की सह-प्रवेश सुविधा दी जाए, और भ्रष्टाचार उजागर करने वाले अधिकारियों को कानूनी सुरक्षा दी जाए।
पर असली सुधार तभी होगा जब राजनीतिक इच्छा शक्ति ईमानदार हो। यह केवल प्रशासनिक नहीं, नैतिक प्रश्न है। जब आम नागरिक ईमानदारी से कर चुकाता है और अधिकारी उस कर से अपनी संपत्तियाँ बनाते हैं, तब शासन का नैतिक आधार ही टूट जाता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी को “दूसरी आज़ादी” कहा था, पर लखनऊ घोटाले ने इसे “दूसरा विश्वासघात” बना दिया है। यह उस वादे की अवहेलना है जिसमें जनता से कहा गया था कि अब भ्रष्टाचार नहीं होगा, केवल विकास होगा। लेकिन आज आम करदाता के मन में यही प्रश्न है — अगर उसका कर धन विकास के बजाय भ्रष्टाचार की जमीन में गाड़ा जा रहा है, तो यह आज़ादी आखिर किसके लिए थी?
“ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा” केवल एक नारा नहीं था, बल्कि एक सामाजिक अनुबंध था। लखनऊ घोटाले ने उस अनुबंध को तोड़ दिया है। जब तक जवाबदेही वास्तविक नहीं बनती, तब तक जीएसटी “गुड एंड सिंपल टैक्स” नहीं, बल्कि “ग्रेट स्कैम इन ट्रांजिशन” ही रहेगा — एक ऐसा कर, जो जनता से वसूला गया और व्यवस्था ने चुपचाप निगल लिया।