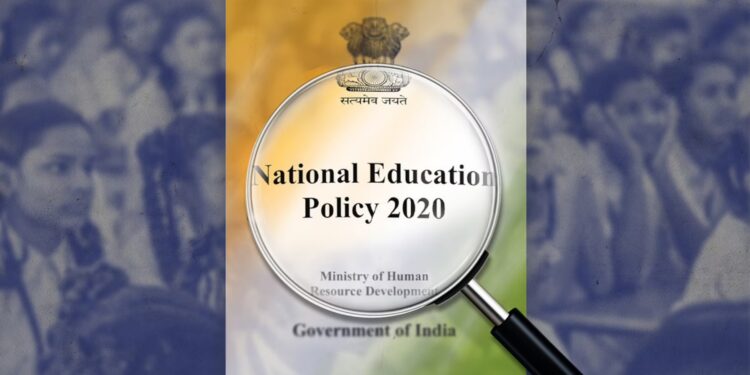लेखक: अमित पांडेय
सुधार के नाम पर देश को फिर से लिखा जा रहा है—उसकी आत्मा को नीतियों की भाषा और डिजिटल डैशबोर्ड्स में कैद किया जा रहा है। जैसे जीएसटी को एक क्रांति बताया गया था—एक ऐसी आग जो भ्रष्टाचार को भस्म कर देगी और पूरे देश को एक बाजार में बदल देगी—उसी तरह अब शिक्षा के नाम पर एक नया मन्त्र फूंका गया है: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025। कहा जा रहा है कि यह एक नया सवेरा है, एक नई पाठ्यचर्या, एक नया भारत। लेकिन इन नारों के पीछे एक ऐसी चुप्पी है जो बहुत कुछ कहती है।
“किसी भी मोड़ पे तुमसे वफादारी नहीं होगी,
हमें मालूम है तुमको ये बीमारी नहीं होगी।”
— मुनव्वर राणा
जब शिक्षा को केवल क्रेडिट्स और इंटर्नशिप्स में तौला जाए, जब बच्चों की कल्पना शक्ति को कोडिंग और एआई मॉड्यूल में समेट दिया जाए, और जब 89,000 स्कूलों को बंद कर दिया जाए—तो क्या हम वास्तव में किसी नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, या बस एक पुराने वादे को नई भाषा में दोहरा रहे हैं?
हरियाणा सरकार का ‘चिराग योजना’ मॉडल, जिसमें सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए ₹500 वसूले जाते हैं जबकि प्राइवेट स्कूलों को ₹1100 की सब्सिडी दी जाती है, यह बताता है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। क्या यह सुधार है या सार्वजनिक शिक्षा से पीछे हटना? अगर सरकारी स्कूल ही चार्ज कर रहे हैं और निजी स्कूलों को सब्सिडी मिल रही है, तो इसका सीधा अर्थ है कि शिक्षा धीरे-धीरे बाजार के हवाले की जा रही है।
नीति कहती है कि परिणाम 2047 तक दिखेंगे। लेकिन जो बच्चा 2025 में स्कूल छोड़ देगा, उसके लिए 2047 क्या मायने रखता है? जो शिक्षक अभी भी ट्रेनिंग का इंतजार कर रहा है, उसका क्या होगा? वह गांव, जहां आज तक स्मार्ट क्लासरूम नहीं पहुंचा, उसकी हिस्सेदारी इस “विकसित भारत” में कहां है?
नीति के वास्तुकार कौन हैं? ऐसे कुलपति और निदेशक जिन्हें न तो योग्यता के आधार पर नियुक्त किया गया है, न अनुभव के बल पर, बल्कि राजनीतिक या वैचारिक निकटता के कारण। क्या यही है बदलाव का मापदंड? जब योग्यता को दरकिनार कर दी जाती है, तब नीति कितनी भी चमकदार क्यों न हो, उसका आधार खोखला होता है।
डिजिटल शिक्षा, हाइब्रिड क्लासरूम, और एआई-आधारित शिक्षण जैसी योजनाएं सुनने में भले ही आधुनिक और उन्नत लगें, लेकिन ग्रामीण भारत के 60% से अधिक घरों में इंटरनेट की सुविधा ही नहीं है। ऐसे में ये डिजिटल प्रयास क्या वास्तव में शिक्षा को पहुंचा रहे हैं, या बस एक और दीवार बना रहे हैं? तकनीक को जब बुनियादी असमानताओं पर थोप दिया जाता है, तो वह सेतु नहीं बनती—वह खाई बन जाती है।
एनईपी 2025 में कक्षा 6 से ही वोकेशनल शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है, जिससे छात्र शुरू से ही “जॉब-रेडी” बनाए जा सकें। लेकिन कई शिक्षाविदों का मानना है कि इससे अमीर छात्रों को खोज और प्रयोग की आज़ादी मिलेगी, जबकि गरीब छात्रों को केवल रोज़गार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। डॉ. कृष्ण कुमार ने इसपर टिप्पणी करते हुए कहा, “अगर अमीरों के लिए शिक्षा खोज है और गरीबों के लिए नौकरी की ट्रेनिंग, तो हम एक नहीं दो देश बना रहे हैं।”
शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व की बात करें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और एनसीईआरटी जैसी संस्थाएं जिनपर इस नीति को लागू करने की जिम्मेदारी है, वे खुद संसाधनों और स्वायत्तता की कमी से जूझ रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, देश के कई राज्यों में 20% से अधिक शिक्षकों की पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है, और जहां शिक्षक हैं भी, उनमें से बहुतों ने कभी स्मार्टबोर्ड देखा तक नहीं है। जब संसाधन ही नहीं हैं, तो नई शिक्षा पद्दति कैसे लागू होगी?
नीति में कहा गया है कि 2026 तक 5+3+3+4 प्रणाली पूरी तरह लागू हो जाएगी, 2027 तक 50% सरकारी स्कूलों में हाइब्रिड क्लासरूम होंगे, और 2030 तक उच्च शिक्षा में सार्वभौमिक पहुंच होगी। लेकिन इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोई ठोस कार्य योजना नहीं दिखती। ₹12,926 करोड़ का बजट 28 राज्यों और हजारों संस्थानों में कैसे कारगर होगा, यह सवाल बना हुआ है।
इस सब के बीच सबसे बड़ा छलावा है 2047 की तारीख। हर योजना, हर नीति, हर जवाब को 2047 पर डाल दिया गया है। जैसे वर्तमान का कोई मोल नहीं, और भविष्य किसी वादे की पोटली है जिसे खोलना सिर्फ सरकार जानती है। लेकिन बच्चे 2047 का इंतजार नहीं कर सकते। वे आज स्कूल में हैं या स्कूल से बाहर। शिक्षक आज कक्षा में खड़े हैं या नौकरी की प्रतीक्षा में। और देश को आज शिक्षा की जरूरत है, वादों की नहीं।
शिक्षा एक सेवा नहीं, एक सामाजिक अनुबंध है। जब सरकार इस अनुबंध को निजी संस्थानों को सौंप देती है, तो सबसे बड़ा नुकसान उन बच्चों को होता है जो पहले से ही समाज की परिधि पर हैं। सरकारी स्कूलों के बंद होने का अर्थ केवल एक कक्षा का खत्म होना नहीं है—वह एक समुदाय का उजड़ जाना होता है।
एनईपी 2025 कागज़ पर एक शानदार दस्तावेज़ है—नई सोच, नई दिशा, नई संभावनाओं से भरा हुआ। लेकिन ज़मीनी हकीकत में यह एक और भाषण बनकर रह जाने का खतरा लिए हुए है। जब तक सार्वजनिक शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी जाती, जब तक शिक्षकों को सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, सम्मान और संसाधन भी नहीं मिलते, और जब तक नीतियों की जवाबदेही तय नहीं होती—तब तक यह नीति भी जीएसटी की तरह एक अच्छा विचार लेकिन खराब अमल बनकर रह जाएगी।
2047 तक का रास्ता प्रतीक्षा कक्ष नहीं हो सकता। बच्चों को वादों से नहीं, अवसरों से पढ़ना होता है। और वे अवसर आज चाहिए—अभी चाहिए।