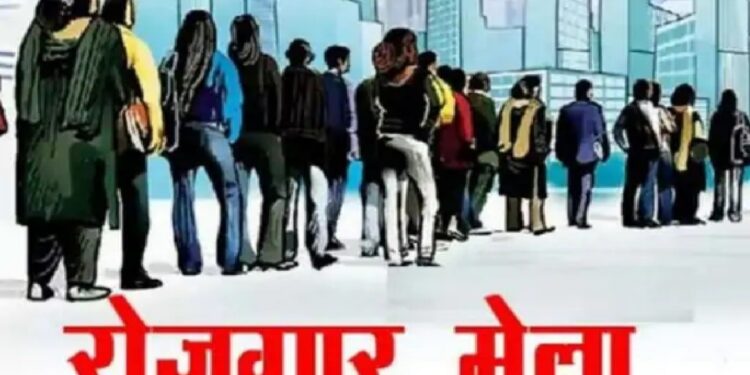2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तो देश के युवाओं को एक नई उम्मीद जगी। घोषणा थी कि हर साल दो करोड़ नौकरियाँ दी जाएँगी। यह वादा न सिर्फ आंकड़ों में बड़ा था, बल्कि देश के करोड़ों शिक्षित बेरोज़गार युवाओं के लिए उम्मीद की एक किरण भी था। लेकिन दस साल बाद, ज़मीन पर जो तस्वीर उभरती है, वह हताशा, प्रतीक्षा और अविश्वास की है।
इन वर्षों में केंद्र सरकार और भाजपा-शासित राज्यों ने कई मंचों पर रोज़गार मेले आयोजित किए। इन मेलों को बड़े विज्ञापनों और प्रधानमंत्री के संबोधनों से भव्य रूप दिया गया, जिसमें चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। देखने में यह सब कुछ प्रेरणादायक प्रतीत होता है, लेकिन जब हम तथ्यों, आँकड़ों और नीतिगत विफलताओं की परतें खोलते हैं, तो सामने आता है एक सुनियोजित छलावा — रोज़गार का भ्रम, जिसमें नौकरियों की बजाय सिर्फ प्रचार और प्रचारकों की जीत होती है।
2022 में शुरू हुए ‘रोज़गार मेले’ का उद्देश्य था सरकारी नियुक्तियों को गति देना और युवाओं को उनके सपनों की नौकरी तक पहुँचाना। अब तक सरकार दावा करती है कि 10 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र बाँटे जा चुके हैं। हाल ही में जुलाई 2025 में 51,000 नियुक्तियों के साथ एक और चरण पूरा हुआ। इन मेलों को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करते हैं, जिनके शब्द होते हैं — “रोज़गार मेला युवाओं को सशक्त करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।”
लेकिन वास्तविकता इससे बहुत दूर है। एक ओर सरकार रोज़गार देने के बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर IndiaTracker जैसे डेटा स्रोत बताते हैं कि 2014 से 2022 के बीच केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए लगभग 22 करोड़ आवेदन आए, जिनमें से केवल 7.22 लाख को ही नियुक्ति मिली। यह सफलता दर 0.03% से भी कम है।
2018–19 में, जब पाँच करोड़ आवेदन आए, तब केवल 38,100 नौकरियाँ दी गईं। यही नहीं, कई बार जिन पदों की नियुक्ति मेलों में की गई, वे पहले से ही स्वीकृत पद होते हैं, जिन्हें केवल औपचारिकता के तहत दोबारा प्रचारित किया जाता है।
विपक्षी नेता राहुल गांधी ने इन मेलों को “रोज़गार के नाम पर इवेंट मैनेजमेंट” बताया। प्रियंका गांधी ने इसे युवाओं के साथ “क्रूर मज़ाक” कह कर आलोचना की। प्रसिद्ध श्रम विशेषज्ञ डॉ. आर. नागराज भी मानते हैं कि “रोज़गार मेला एक प्रतीकात्मक आयोजन है, जो जमीनी रोज़गार संकट को नहीं सुलझा सकता।”
प्रशासनिक संकट और युवाओं का टूटता भरोसा
सिर्फ नियुक्तियों की संख्या ही नहीं, बल्कि भर्ती प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता पर भी गहरा संकट मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 में लीक हो गई, जिससे 48 लाख उम्मीदवार प्रभावित हुए। राजस्थान में पिछले एक दशक में 14 से अधिक बड़े पेपर लीक सामने आए। यूपीपीसीएस, शिक्षक पात्रता परीक्षा, और रीट जैसी प्रमुख परीक्षाएँ लगातार धांधली की भेंट चढ़ी हैं।
इससे युवाओं में एक गहरी निराशा फैली है। लाखों छात्र वर्षों की मेहनत के बाद पेपर लीक के कारण खुद को ठगा महसूस करते हैं। एक प्रतियोगी छात्र की बात इसका प्रतीक है: “हमारी तैयारी बिक चुकी है।”
हालाँकि, सरकार ने 2024 में ‘पब्लिक एग्ज़ामिनेशन (अनफेयर मीन्स की रोकथाम) अधिनियम’ पारित कर इस पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि कानून विश्वास नहीं लौटाते, वह तो व्यवस्था की पारदर्शिता और भरोसे से आता है।
इसके अलावा, सरकारी स्कूलों की बंदी भी एक गंभीर मुद्दा है। 2014 से अब तक 89,000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद किए जा चुके हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में चतुर्थ श्रेणी की नौकरियाँ — जैसे सफाईकर्मी, चपरासी, रसोइया — गायब हो गईं। यही वे नौकरियाँ थीं, जो गांवों में युवाओं को आर्थिक सहारा देती थीं।
सरकारी संस्थाओं में अब भर्ती के नाम पर ठेके की व्यवस्था चल रही है, जिसमें PRD, UPNAL, BASIL जैसी एजेंसियाँ नियुक्तियाँ करती हैं। ये नौकरियाँ स्थायी नहीं होतीं, न ही इनमें भविष्य की कोई सुरक्षा होती है। इससे एक ऐसा मज़दूर वर्ग तैयार हुआ है जो न ठेठ सरकारी है, न निजी — बल्कि बस अस्थायी है और असहाय।
सरकारी नीतियों में अब विकास की बजाय प्रचार की प्राथमिकता दिखने लगी है। रोज़गार मेलों पर अब तक 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए जा चुके हैं — यह खर्च मुख्यतः विज्ञापनों, वीडियो संदेशों, पोस्टर-बैनर, और डिजिटल प्रचार पर हुआ है। यानी, नौकरी से पहले प्रचार पहुँचता है।
सरकार ने ‘स्किल इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’, जैसे कार्यक्रम शुरू तो किए, लेकिन प्रशिक्षण और रोज़गार के बीच का फासला अब भी उतना ही चौड़ा है। युवाओं को कौशल तो मिल रहा है, लेकिन नौकरियाँ नहीं। संसदीय समिति ने 2023 में माना कि कई प्रशिक्षित युवा ऐसे क्षेत्र में नौकरी करते हैं, जहाँ उनके कौशल की कोई आवश्यकता ही नहीं होती — या फिर उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती।
ग्रामीण भारत में अब भी लाखों युवा मनरेगा में मज़दूरी करने को मजबूर हैं — यह संकेत है कि देश की अर्थव्यवस्था में स्थायी नौकरियाँ नहीं, बल्कि विकल्पहीन श्रम बढ़ रहा है।
वादे नहीं, योजना चाहिए — युवाओं को अधिकार दो, कृपा नहीं
रोज़गार मेलों में बाँटे जाने वाले नियुक्ति पत्र अधिकतर पहले से स्वीकृत पदों के लिए होते हैं। इनमें न नौकरी की स्थायित्वता की गारंटी होती है, न पदोन्नति का कोई स्पष्ट रास्ता। सरकार जिस तरह से इन मेलों को प्रचारित करती है — जैसे कोई चुनावी विजय हो — वह दर्शाता है कि रोज़गार अब एक नीति नहीं, एक ‘इवेंट’ बन चुका है।
2015 में भारतीय श्रम सम्मेलन ने राष्ट्रीय रोज़गार नीति की अनुशंसा की थी, जिसे आज तक लागू नहीं किया गया। एक ऐसी नीति की आवश्यकता है जो —
• राज्यों को उनके स्तर पर नियुक्ति का अधिकार दे,
• कौशल और बाज़ार की माँग को जोड़ सके,
• और रोज़गार को ‘सहायता’ नहीं, संवैधानिक अधिकार मान सके।
संविधान के नीति निदेशक तत्वों में कहा गया है कि राज्य नागरिकों को ‘कार्य का अधिकार’ सुनिश्चित करेगा। लेकिन आज रोजगार को सरकार एक कृपा की तरह पेश कर रही है — जैसे युवाओं को नौकरी मिलना उनकी योग्यता से नहीं, सत्ता की मेहरबानी से तय हो।