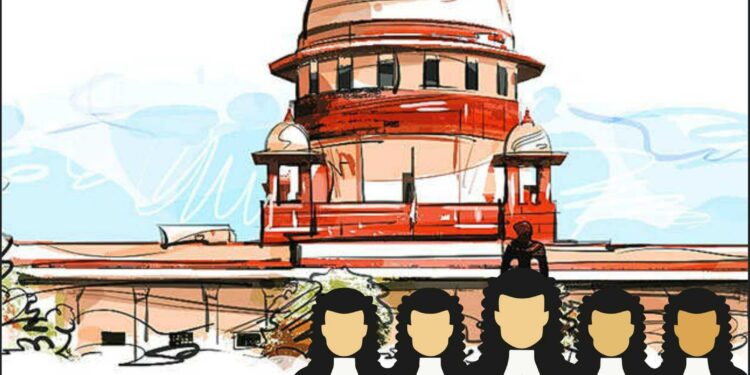Judicial Appointments in India: वर्तमान में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच विवाद बढ़ता दिख रहा है । विवाद की शुरुवात तो दशकों पहले न्यायपालिका और भारतीय लोकतंत्र के अन्य दो स्तंभ – विधायिका, कार्यपालिका के बीच उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति के सवाल को लेकर हो गई थी । इन तीनों की स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व भारतीय संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। लेकिन जब न्यायपालिका स्वयं ही न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के प्रावधानों में दी गई व्यवस्था से अलग जाकर करने लगे, तो यह सवाल उठता है कि क्या यह व्यवस्था न्यायसंगत और संविधान सम्मत है? क्या यह ‘स्व-नियुक्ति’ प्रणाली पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर खरी उतरती है? यह प्रश्न विशेष रूप से कोलेजियम प्रणाली और उसके आसपास उठते विवादों के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण हो जाता है।
वर्तमान में भारत में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से होती है। यह प्रणाली संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं लिखी गई है, बल्कि यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों से विकसित हुई है, जिसे “तीन जजों के मामले” (Three Judges Cases) के नाम से जाना जाता है।
तीन जजों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि जजों की नियुक्ति को कोलेजियम प्रणाली से किया जाएगा जिसमें मुख्य न्यायाधीश और चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की समिति द्वारा जजों की नियुक्तियों , स्थानांतरण आदि में इस कोलिजियम की सिफारिश को अंतिम माना जाएगा जबकि संविधान की धारा 124 में सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं कुछ अन्य वरिष्ठ जजों से राय मशविरा किए जाने की व्यवस्था दी गई है और नियुक्ति विषयक अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को दिया गया था।
हालांकि कोलेजियम प्रणाली को लाते समय यही कहा गया था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है , लेकिन इसके खिलाफ कई आलोचनाएँ सामने आई हैं जिस में सब से प्रमुख तर्क पारदर्शिता का अभाव माना गया क्योंकि कोलेजियम की सिफारिशें गोपनीयता में होती हैं , उनके मानदंड स्पष्ट नहीं होते, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही पर प्रश्नचिन्ह लगते हैं। इसके अतिरिक्त जनता या संसद को कोलेजियम के निर्णयों को चुनौती देने या उनकी समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं होता, जिससे लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व कम होता है। कोलिजियम व्यवस्था से किए गए चयन के ऊपर समय समय पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि कोलेजियम प्रणाली में निजी सिफारिशें, जान-पहचान और क्षेत्रीय पक्षपात के आधार पर नियुक्तियाँ होती हैं जिस पर कभी भी कोई सफ़ाई प्रस्तुत किए जाने का साक्ष्य नहीं है और ना ही इस प्रकार की शिकायतों की कोई जाँच पड़ताल की गई हो, ऐसा प्रतीत होता है ।
संविधान निर्माताओं ने न्यायिक नियुक्तियों में संतुलन की कल्पना की थी, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और राष्ट्रपति की भूमिकाएं परस्पर पूरक हों। लेकिन कोलेजियम प्रणाली इस संतुलन को न्यायपालिका के पक्ष में झुका देती है, जो लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों से मेल नहीं खाती। 2014 में संसद ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम (NJAC Act) पारित किया, जिसका उद्देश्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाना था। लेकिन 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट का मानना था कि NJAC न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकता है।
स्पष्टः कोई भी कानून परफेक्ट नहीं होता और समय के साथ उसमें संशोधन या सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है । इसी प्रकार NJAC भी पूर्णतः त्रुटिरहित हो ऐसा नहीं कहा जा सकता और उसमें में भी कुछ खामियाँ थीं, लेकिन यह पारदर्शिता और सार्वजनिक सहभागिता की दिशा में एक कदम था। कोलिजियम प्रणाली को लाने के पीछे सबसे बड़ा तर्क यह दिया गया था कि उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ गया है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाये रखने में बाधा पैदा कर रहा । तर्क यह दिया गया कि पॉलिटिशियनस ग़लत लोगों को चुन कर अपनी मर्जी के लोगों को जज नियुक्त करा कर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं । प्रश्न यह है कि जब जज लोग ही कोलीजियम सिस्टम से ग़लत जज चुनने लगे तो क्या उससे न्यायपालिका का पूरा सिस्टम ख़राब नहीं होता ? ऐसे हालात में स्थिति में कैसे सुधार किया जाना चाहिए जब जनता जो कि लोकतंत्र में सर्वोच्च होती है उसके द्वारा चुने गए पदाधिकारियों की जजों की नियुक्ति में संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुसार दी गई भागीदारी ही कोलिजियम व्यवस्था द्वारा छीन ली गई हो ।
हाल में ही न्यायपालिका की साख पर सब से ज़्यादा चोट तब पंहुँची जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के घर से करोड़ों रुपए मिलने का मामला सामने आया जिस पर कोई कठोर और त्वरित कार्यवाही करने के बजाय मामले को ठण्डे बस्ते में डालने जैसी कार्यवाही की गई । दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत सिंह के मामले में क्या जनता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि वर्मा जी के घर में जले पचास करोड़ कहाँ से आये और वर्मा जी से कोई खुली पूँछताछ क्यों नहीं हो रही । क्या जज देश के क़ानून से ऊपर हैं , क्या उनको भी जाँच एजेंसी के सामने जाकर निष्पक्ष जाँच पड़ताल में शामिल नहीं होना चाहिए ? जजों को सभी क़ानूनों से ऊपर किसने कब कर दिया ? हर छोटे बड़े भ्रष्टाचार पर सीबीआई जांच का आदेश जारी करने वाले जुडिसियल सिस्टम के पुरोधा लोग एक हाई कोर्ट के जज के घर से पचास करोड़ के नोटों के जखीरे मिलने के इस खुले भ्रष्टाचार के मामले पर चुप्पी क्यों साधे हैं ? अपराध के मामले में आंतरिक जांच का प्रावधान देश की पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किस क़ानून में है , इसको देश के लिए जानना बहुत ज़रूरी है । ऐसे गंभीर मामले में लीपापोती देश को भ्रष्टाचार के और गहरे गड्ढे में धकेल देगा क्योंकि आगे आने वाले समय में न्यायपालिका भ्रष्टाचार के मामले पर कुछ भी कर पाने का नैतिक बल खो देगी ।
एक विचारणीय प्रश्न यह भी है कि जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जनता की सुरक्षा , देश की सुरक्षा , एटम बम बनाने या ना बनाने , दूसरे देश से युद्ध या शांति का निर्णय , देशी और विदेशी व्यापार , सभी आर्थिक मामलों , जनता के लिए रोज़गार , भोजन , शिक्षा , स्वास्थ संबंधी सभी निर्णय लेने के लिए सक्षम है तो क्या वह कुछ जजों की नियुक्ति को ठीक ढंग से कर पाने के लिए अक्षम घोषित की जा सकती है ? यह अधिकार कुछ जज स्वयं ही निर्णय देकर नियुक्ति का अधिकार अपने पास रखने पर जिद क्यों करते हैं , यह आम जन की समझ के बाहर है ।
इस विवाद का स्थायी समाधान न्यायिक नियुक्ति प्रणाली को पारदर्शी, उत्तरदायी और संतुलित बनाकर ही संभव है। इसके लिए कोलीजियम व्यवस्था को समाप्त करके संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुसार ही खुले मन से इस मामले से संबंधित पक्ष सरकार , न्यायपालिका एक साथ बैठ कर अपने अपने पक्ष के तर्कों पर विचार करते हुए देश हित में अपनी प्रतिष्ठा के प्रश्न को दर किनार करते हुए एक ऐसी संविधान परक व्यवस्था तैयार करें जिसके माध्यम से केवल सक्षम , ईमानदार लोगों की ही उच्च स्तरीय न्यायिक पदों पर नियुक्ति संभव हो सके। यह कार्य बिल्कुल मुश्किल नहीं है ।
न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह स्वयं के लिए पूरी तरह से बंद प्रणाली विकसित करे। भारत जैसे लोकतंत्र में जहाँ पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जनता की भागीदारी प्रमुख मूल्य हैं, वहाँ न्यायाधीशों की नियुक्ति एक संतुलित, संवैधानिक और खुली प्रक्रिया से ही होनी चाहिए। कोलेजियम प्रणाली पर वर्षों से उठ रहे प्रश्नों को अब दबाया जाना देश हित में नहीं होगा ।
(विजय शंकर पांडे भारत सरकार के पूर्व सचिव हैं)